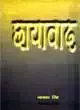|
लेख-निबंध >> नामवर सिंह संकलित निबंध नामवर सिंह संकलित निबंधनामवर सिंह
|
162 पाठक हैं |
||||||
नामवर सिंह : संकलित निबंध हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह के प्रतिनिधि निबंधों व समालोचनाओं का संकलन है।...
नामवर सिंह : संकलित निबंध हिंदी आलोचना के
शिखर पुरुष नामवर सिंह के प्रतिनिधि निबंधों व समालोचनाओं का संकलन है। अपने समय के प्रश्नों से टकराते हुए युगचेतना से संपृक्त एक बेहद जागरुक आलोचक की विश्लेषण क्षमता, साहित्य के मर्म की गहरी समझ और तथ्यों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने की उनकी अभिनव शैली को यहां समझा जा सकता है। नामवर सिंह साहित्य की सापेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए उसके
सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष को भी महत्व देते हैं और उसका ऐतिहासिक संदर्भों
में मूल्यांकन करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से साहित्य, समाज, इतिहास और
संस्कृति से जुड़ी उनकी चिंताओं से अवगत हुआ जा सकता है।
नामवर सिंह (जन्म : 1927, जीयनपुर, बनारस) भारतीय साहित्य के गौरव पुरुष हैं। सन् 1956 में बीएचयू से पीएच.डी. करने के बाद वे बनारस, सागर, जोधपुर, आगरा में अध्यापन कार्य करते हुए 1974 में जेएनयू आए और 18 वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक रहे। भारतीय भाषा केन्द्र, जेएनयू के संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष रहे प्रो. नामवर सिंह अपनी सेवानिवृत्ति, इतिहास और आलोचना, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, कहानी : नई कहानी, पृथ्वीराज रासो : भाषा और साहित्य, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक प्रो. सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और हैदराबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. की मान उपाधि से अलंकृत किया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्तमान कुलाधिपति प्रो. नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं।
नामवर सिंह (जन्म : 1927, जीयनपुर, बनारस) भारतीय साहित्य के गौरव पुरुष हैं। सन् 1956 में बीएचयू से पीएच.डी. करने के बाद वे बनारस, सागर, जोधपुर, आगरा में अध्यापन कार्य करते हुए 1974 में जेएनयू आए और 18 वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक रहे। भारतीय भाषा केन्द्र, जेएनयू के संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष रहे प्रो. नामवर सिंह अपनी सेवानिवृत्ति, इतिहास और आलोचना, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, कहानी : नई कहानी, पृथ्वीराज रासो : भाषा और साहित्य, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक प्रो. सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और हैदराबाद विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट. की मान उपाधि से अलंकृत किया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्तमान कुलाधिपति प्रो. नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के प्रधान संपादक भी हैं।
केवल मैं केवल मैं
हिन्दी काव्य की पूरी परंपरा का अनुशीलन करते हुए जैसे ही कोई पाठक
छायावाद की सीमा में प्रवेश करता है, ये कविताएं तुरंत अपनी आत्मीयता से
उसे आकृष्ट कर लेती हैं। वहाँ वह देखता है कि कवि निर्वैयक्तिकता का सारा
आवरण उतारकर एक आत्मीयक की भांति अत्यंत निजी ढंग से बातें कर रहा है।
यहां हृदय के भाव किसी कल्पित कहानी अथवा पौराणिक पुरुषों के माध्यम की
अपेक्षा नहीं रखते। अपने मन की बातें कवि सीधे-सीधे अपने ही मुख से उत्तम
पुरुष में कह रहा है और पाठक को इस तरह उन भावों के साथ तादात्म्य अनुभव
करने में बड़ी सुगमता होती है। इससे कवि और पाठक के बीच परस्पर सुखद
अनूभूति होती है।
लेकिन कवि ने यह जो ‘मैं शैली’ अपनाई, वह केवल शैली भर नहीं है। इस निजता और आत्मीयता के पीछे आधुनिक युवक का पूरा व्यक्तित्व है, जो अपने को सीधे-सीधे अभिव्यक्त करने की सामाजिक स्वाधीनता चाहता है। यदि कहानी के पात्रों अथवा पौराणिक व्यक्तियों के माध्यम से वह अपनी बातें कह सकता है तो अवश्य कहता क्योंकि अभिव्यक्ति की यह नाटकीय प्रणाली चिराचरित और अनुभवसिद्ध है। लेकिन उसे लगा कि अपनी बात निजी ढंग से ही वह अच्छी तरह कह सकता है। उसकी वैयक्तिकता पुरानी निर्वैयक्तिकता में घुट-सी रही थी। निर्वैयक्तिकता में उसे एकदम आत्म-निषेध की आशंका थी। रीतिकाल के कवियों की ‘रूढ़िगत तटस्थता’ उसके लिए असह्य प्रतीत हो रही थी। इसलिए यह वैयक्तिक अभिव्यक्ति कवि के लिए व्यक्ति की मुक्ति थी। पूर्ववर्ती कविता की निर्वैयक्तिकता की तुलना में यह वैयक्तिकता का आग्रह कितना बड़ा विद्रोह था, उसका अनुमान तत्कालीन पुराण-पंथी पंडितों की आलोचनाओं से कुछ-कुछ हो सकता है।
मध्ययुग में भक्त कवियों ने केवल आत्म-निवेदन में इस आत्मीयता-पद्धति का सहारा लिया है और इसीलिए कबीर और मीरा के आत्मनिवेदनों तथा सूर-तुलसी के विनय-पदों में लोगों ने अधिक तन्मयता अनुभव की है। भक्तों के उन आत्म-निवेदनों से स्पष्ट है कि अपने भगवान से जहां उन्हें सीधी बात करनी थी, वहां उन्होंने संपूर्ण तटस्थता का परित्याग करके एकदम आमने-सामने बातचीत की है। भावावेद की स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वाभाविक परिणति यही है। उस युग में यह बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन आधुनिक युग की वैयक्तिक अभिव्यक्ति भक्तों के आत्म-निवेदन से कहीं अधिक आगे की चीज़ है। भक्तों ने जो आत्म-निवेदन किया उस पर धर्म का आवरण था और धर्म का यह आवरण ही उसे तटस्थता प्रदान करने के लिए काफ़ी था। लेकिन आधुनिक विज्ञान तथा उससे प्रभावित सामाजि, राजनीतिक तथा नैतिक मान्यताओं ने तो नई पीठी के मन से वह धार्मिक आवरण भी एक हद तक उतार फेंका। मध्ययुग की धार्मिकता का स्थान आधुनिका युग की ऐतिहकता ने ले लिया। फलतः छायावादी कवि की वैयक्तिक अभिव्यक्ति के लिए इस ऐहिक युग में कोई आवरण नहीं रह गया। प्राचीन मर्यादा के रक्षकों के लिए यह नग्न और ऐहिक वैयक्तिकता कितनी अरुचिकर प्रतीत हुई, यह उनके तत्कालीन विरोधों से ही प्रकट है।
पुराना कवि अपने निजी प्रणय-संबंध को सीधे ढंग से व्यक्त करने में असमर्थ था। रीतिकाल के कवियों के लिए भी राधा-कन्हाई की ओट अनिवार्य थी। सामती नैतिकता का बंधन पड़ा था ! लेकिन इस बंधन को अस्वीकार करते हुए पंत ने ‘उच्छ्वास’ और आंसू’ की बालिका के प्रति सीधे शब्दों में अपना प्रणय प्रकट किया और यह निश्चित है कि ‘उच्छवास्’ की सरल बालिका कोई रहस्यात्मक शक्ति नहीं है। उसके विषय में कवि की स्पष्टोक्ति है : ‘बालिका मेरी मनोरम मित्र थी।’
कवि ने समाज से यह छूट पहली बार ली। और ध्यान देने की बात है कि इसके लिए कवि कहीं भी अपने को अपराधी अथवा हीन अनुभव नहीं करता। अपनी दुर्बलताओं को वह उसी प्रकार खोलकर रखता है, जिस प्रकार अपने प्रेम की पावनता को दृढ़ता के साथ प्रमाणित करता है। उसे इस कार्य में कहीं भी अनैतिकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि वह जानता है कि यह तो मानवीयता अथवा मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है।
कविता में जहां देवताओं के प्रेम का वर्णन होता था, वह स्थान साधारण मनुष्य ले ले—यह जनतांत्रिक भाव की विजय है; यह मध्यवर्ग की पहली सामाजिक स्वाधीनता है।
जब यह सामाजिक स्वाधीनता प्रणय के क्षेत्र में ली गई तो इसका प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। निराला ने अपनी पुत्री ‘सरोज’ की स्मृति में शोकगती लिखा और उसमें अपने निजी जीवन की अनेक बातें साफ़-साफ़ कह डालीं। संपादकों द्वारा मुक्त छंद की रचनाओं का लौटाया जाना, विरोधियों के शब्दिक प्रहार, मातृहीन लड़की का ननिहाल में पालन-पोषण, दूसरे विवाह के लिए निरंतर आते हुए प्रस्ताव और उन्हें ठुकराना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एकदम नए ढंग से कन्या का विवाह करना, उचित दवा-दारू के अभाव में सरोज का देहावसान और उस पर कवि का शोकोद्गार। यह सब पंत के ‘उच्छ्वास’ और ‘आंसू’ की वैयक्तिकता से हज़ार डग आगे है। कविता क्या है, कवि की पूरी आत्मकथा है; इसमें जो शेष रहा, वह ‘वन-बेला’ में पूरा हो गया। यहां केवल आत्म-खता नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक-एक कर पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और आधुनिक अर्थ-पिशाचों पर प्रहार किया गया है। यदि एक ओर कवि अपने कनौजिया बंधुओं को इन शब्दों में याद करता है :
लेकिन कवि ने यह जो ‘मैं शैली’ अपनाई, वह केवल शैली भर नहीं है। इस निजता और आत्मीयता के पीछे आधुनिक युवक का पूरा व्यक्तित्व है, जो अपने को सीधे-सीधे अभिव्यक्त करने की सामाजिक स्वाधीनता चाहता है। यदि कहानी के पात्रों अथवा पौराणिक व्यक्तियों के माध्यम से वह अपनी बातें कह सकता है तो अवश्य कहता क्योंकि अभिव्यक्ति की यह नाटकीय प्रणाली चिराचरित और अनुभवसिद्ध है। लेकिन उसे लगा कि अपनी बात निजी ढंग से ही वह अच्छी तरह कह सकता है। उसकी वैयक्तिकता पुरानी निर्वैयक्तिकता में घुट-सी रही थी। निर्वैयक्तिकता में उसे एकदम आत्म-निषेध की आशंका थी। रीतिकाल के कवियों की ‘रूढ़िगत तटस्थता’ उसके लिए असह्य प्रतीत हो रही थी। इसलिए यह वैयक्तिक अभिव्यक्ति कवि के लिए व्यक्ति की मुक्ति थी। पूर्ववर्ती कविता की निर्वैयक्तिकता की तुलना में यह वैयक्तिकता का आग्रह कितना बड़ा विद्रोह था, उसका अनुमान तत्कालीन पुराण-पंथी पंडितों की आलोचनाओं से कुछ-कुछ हो सकता है।
मध्ययुग में भक्त कवियों ने केवल आत्म-निवेदन में इस आत्मीयता-पद्धति का सहारा लिया है और इसीलिए कबीर और मीरा के आत्मनिवेदनों तथा सूर-तुलसी के विनय-पदों में लोगों ने अधिक तन्मयता अनुभव की है। भक्तों के उन आत्म-निवेदनों से स्पष्ट है कि अपने भगवान से जहां उन्हें सीधी बात करनी थी, वहां उन्होंने संपूर्ण तटस्थता का परित्याग करके एकदम आमने-सामने बातचीत की है। भावावेद की स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वाभाविक परिणति यही है। उस युग में यह बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन आधुनिक युग की वैयक्तिक अभिव्यक्ति भक्तों के आत्म-निवेदन से कहीं अधिक आगे की चीज़ है। भक्तों ने जो आत्म-निवेदन किया उस पर धर्म का आवरण था और धर्म का यह आवरण ही उसे तटस्थता प्रदान करने के लिए काफ़ी था। लेकिन आधुनिक विज्ञान तथा उससे प्रभावित सामाजि, राजनीतिक तथा नैतिक मान्यताओं ने तो नई पीठी के मन से वह धार्मिक आवरण भी एक हद तक उतार फेंका। मध्ययुग की धार्मिकता का स्थान आधुनिका युग की ऐतिहकता ने ले लिया। फलतः छायावादी कवि की वैयक्तिक अभिव्यक्ति के लिए इस ऐहिक युग में कोई आवरण नहीं रह गया। प्राचीन मर्यादा के रक्षकों के लिए यह नग्न और ऐहिक वैयक्तिकता कितनी अरुचिकर प्रतीत हुई, यह उनके तत्कालीन विरोधों से ही प्रकट है।
पुराना कवि अपने निजी प्रणय-संबंध को सीधे ढंग से व्यक्त करने में असमर्थ था। रीतिकाल के कवियों के लिए भी राधा-कन्हाई की ओट अनिवार्य थी। सामती नैतिकता का बंधन पड़ा था ! लेकिन इस बंधन को अस्वीकार करते हुए पंत ने ‘उच्छ्वास’ और आंसू’ की बालिका के प्रति सीधे शब्दों में अपना प्रणय प्रकट किया और यह निश्चित है कि ‘उच्छवास्’ की सरल बालिका कोई रहस्यात्मक शक्ति नहीं है। उसके विषय में कवि की स्पष्टोक्ति है : ‘बालिका मेरी मनोरम मित्र थी।’
कवि ने समाज से यह छूट पहली बार ली। और ध्यान देने की बात है कि इसके लिए कवि कहीं भी अपने को अपराधी अथवा हीन अनुभव नहीं करता। अपनी दुर्बलताओं को वह उसी प्रकार खोलकर रखता है, जिस प्रकार अपने प्रेम की पावनता को दृढ़ता के साथ प्रमाणित करता है। उसे इस कार्य में कहीं भी अनैतिकता नहीं प्रतीत होती, क्योंकि वह जानता है कि यह तो मानवीयता अथवा मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है।
कविता में जहां देवताओं के प्रेम का वर्णन होता था, वह स्थान साधारण मनुष्य ले ले—यह जनतांत्रिक भाव की विजय है; यह मध्यवर्ग की पहली सामाजिक स्वाधीनता है।
जब यह सामाजिक स्वाधीनता प्रणय के क्षेत्र में ली गई तो इसका प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। निराला ने अपनी पुत्री ‘सरोज’ की स्मृति में शोकगती लिखा और उसमें अपने निजी जीवन की अनेक बातें साफ़-साफ़ कह डालीं। संपादकों द्वारा मुक्त छंद की रचनाओं का लौटाया जाना, विरोधियों के शब्दिक प्रहार, मातृहीन लड़की का ननिहाल में पालन-पोषण, दूसरे विवाह के लिए निरंतर आते हुए प्रस्ताव और उन्हें ठुकराना, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एकदम नए ढंग से कन्या का विवाह करना, उचित दवा-दारू के अभाव में सरोज का देहावसान और उस पर कवि का शोकोद्गार। यह सब पंत के ‘उच्छ्वास’ और ‘आंसू’ की वैयक्तिकता से हज़ार डग आगे है। कविता क्या है, कवि की पूरी आत्मकथा है; इसमें जो शेष रहा, वह ‘वन-बेला’ में पूरा हो गया। यहां केवल आत्म-खता नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक-एक कर पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और आधुनिक अर्थ-पिशाचों पर प्रहार किया गया है। यदि एक ओर कवि अपने कनौजिया बंधुओं को इन शब्दों में याद करता है :
ये कान्यकुब्द-कुल कुलांगार
खाकर पत्तल में करें छेद
इनके कर कन्या, अर्थ खेद
खाकर पत्तल में करें छेद
इनके कर कन्या, अर्थ खेद
और फिर गंवार दामाद का यह चित्र :
वे जो जमुना के से कछार
पद फटे बिवाई के, उधार
खाए के मुख ज्यों, पिए तेल
चमरौधे जूते से, सकेल
निकले, जी लेते, घोर-गंध,
उन चरणों को मैं यथा-अंध,
कल घ्राण-प्राण से रहित व्यक्ति
हो पूजूं, ऐसी नहीं शक्ति
पद फटे बिवाई के, उधार
खाए के मुख ज्यों, पिए तेल
चमरौधे जूते से, सकेल
निकले, जी लेते, घोर-गंध,
उन चरणों को मैं यथा-अंध,
कल घ्राण-प्राण से रहित व्यक्ति
हो पूजूं, ऐसी नहीं शक्ति
तो दूसरी ओर वह निरानंद संपादक के गुण
सुन-सुनकर यथाभ्यास पास की घास नोंचता हुआ अज्ञात इधर-उधर फेंकता है। इसी
सिलसिले में उस समाज-व्यवस्था को भी याद किया जाता है जिससे
‘उपार्जन को अक्षम’ कवि अपना कन्या को चीनांशुक
कहवाकर दधिमुख करना तो दूर, कुछ भी न कर सका।
यह निराला ही हैं जो तमाम रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी सद्यःपरिणीता कन्या के रूप का खुलकर वर्णन करते हैं और यह कहना नहीं भूलते कि ‘पुष्प-सेज तेरी स्वयं रची है।’ है किसी कवि में इतना साहस और संयम !
पंत और निराला की तरह आत्माभिव्यक्ति प्रसाद ने भी की। ‘हंस’ के ‘आत्मकथा’ अंक के लिए जब उनके सुहृदय प्रेमचन्द ने ‘आत्मकथा’ लिखने का आग्रह किया तो प्रसाद ने नहीं-नहीं कहते हुए भी आत्मकथा कह ही डाली। कवि ने अपनी दुर्बलताओं की कोई फ़ेहरिस्त पेश नहीं की, फिर भी इतना कह ही दिया कि ‘तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीती।’ जिस संयत हृदय ने ‘अपनी भूलों के नाम ही औरों की प्रवंचना दिखलाने’ से इंकार किया, उसी ने अपने मधुमय जीवन की झांकी देनें में भी संकोच नहीं दिखलाया और कहा कि—
यह निराला ही हैं जो तमाम रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी सद्यःपरिणीता कन्या के रूप का खुलकर वर्णन करते हैं और यह कहना नहीं भूलते कि ‘पुष्प-सेज तेरी स्वयं रची है।’ है किसी कवि में इतना साहस और संयम !
पंत और निराला की तरह आत्माभिव्यक्ति प्रसाद ने भी की। ‘हंस’ के ‘आत्मकथा’ अंक के लिए जब उनके सुहृदय प्रेमचन्द ने ‘आत्मकथा’ लिखने का आग्रह किया तो प्रसाद ने नहीं-नहीं कहते हुए भी आत्मकथा कह ही डाली। कवि ने अपनी दुर्बलताओं की कोई फ़ेहरिस्त पेश नहीं की, फिर भी इतना कह ही दिया कि ‘तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीती।’ जिस संयत हृदय ने ‘अपनी भूलों के नाम ही औरों की प्रवंचना दिखलाने’ से इंकार किया, उसी ने अपने मधुमय जीवन की झांकी देनें में भी संकोच नहीं दिखलाया और कहा कि—
जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में
उसकी स्मृति पाथेय पनी है थके पथिक की पंथा की
सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में
उसकी स्मृति पाथेय पनी है थके पथिक की पंथा की
सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
और ‘अरुण कपोलों’ की इस झलक के बाद उस थके पथिक की
कंथा की सीवन को उधेड़कर देखने का दुस्साहस कोई ऐसा ही निर्मम करेगा जिसकी
दिलचस्पी स्थूल घटनाओं में होगी।
सामंती रूढ़ियोंवाले समाज के सामने जब एक पुरुष की यह स्थिति है, तो इस पुरुष-समाज में नारी के लिए आत्माभिव्यक्ति में कितनी बड़ी कठिनाई हो सकती है,यह सहज अनुमेय है। फिर भी महादेवी वर्मान ने अपने गीतों में वैयक्तिक ढंग से अभिव्यंजना की और इसके लिए उन्होंने कितने प्रवाद झेले, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। महादेवीजी ने कहीं लिखा है कति आज का साहित्यकार अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है।
इतना होते हुए भी सामाजिक रूढ़ियों के प्रहार की आशंका से कवि को वैयक्तिक अनुभूतियों के लिए रहस्यवाद का आश्रय लेना पड़ा। स्थूल धार्मिक आवरण तो वह ले नहीं सकता था, लेकिन ऐहिक वैयक्तिकता की क्षुद्रता से बचाने के लिए रहस्यात्मकता के ऊर्ध्व आसन पर प्रिय को बैठाना ही पड़ा। महादेवी ने नारी होकर ऐसा किया तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष होकर भी प्रसाद ने ‘आंसू’ के दूसरे संस्करण को अत्यधिक रहस्यात्मक और सामाजिक लोक-मंगल-परक बना डाला; जबकि ‘आंसू’ का प्रथम संस्करण शुद्ध ऐहिक प्रेम की विरह-वेदना का काव्य है।
इतना होते हुए भी आलोचकों से वास्तविकता छिपी न रह सकी और शुक्लजी जैसे गंभीर आचार्य भी खुल ही पड़े कि ‘‘इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस-प्रसार के लिए रहस्यवाद का परदा मिल गया अथवा यों कहें कि इनकी नारी प्रणयानुभूति ससी में कूदकर असीम पर जा रही।’’
इस कथन के पीछे और प्रवृत्ति चाहे जो हो, लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि उस युग की पुरानी पीढ़ी के लोग भी छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं को मूलतः कवि की आत्मानुभूति ही मानते थे।
यह आत्माभिव्यक्ति की भावना इस युग में कितनी व्यापक रही है, इसका पता इसी से चलता है कि ‘आत्मकथा’ लिखने की परंपरा सी चल पड़ी। गांधी, नेहरू, रवींद्रनाथ, श्रद्धानंदज, श्यामसुंदरदास, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन आदि न जाने कितने राजनीतिज्ञों, धर्मसुधारकों और साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा अथवा जीवन-स्मृति लिखी है। इतने बड़े पैमाने पर इस देश में आत्मकथाएं पहले शायद ही कभी लिखी गईं। मध्ययुग के हिन्दी साहित्य में केवल एक आत्मकथा मिलती है, बनारसीदास जैन की ‘अर्धकथानक।’
ये आत्मकथाएं इस युग में प्रचलित वैयक्तिक आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा की द्योतक हैं। ये बतलाती हैं कि व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कितना आकुल था ! वह अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहता था। उसकी इस आकांक्षा में स्वाधीनता की कामना थी और अभिव्यंजना में साहस भी। हर देश में ‘रौमैंटिसिज़्म’ का अभ्युदय प्रायः इसी आकांक्षा के साथ हुआ। फ्रांस और फिर पूरे यूरोप में रोमांटिक साहित्य का प्रवर्तन करनेवाले रूसो के ‘कन्फेशन’ के आरंभिक उद्गार से इस भावना के ऐतिहासिक महत्तव का ठीक पता चलता है। रूसो लिखता है :
‘‘आज मैं अपने हाथ में वह कार्य ले रहा हूं, जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया था और न भविष्य में ही कोई करेगा। मैं अपने मित्रों के सामने एक मनुष्य का सच्चा रूप रखना चाहता हूं और वह मनुष्य स्वयं मैं हूं। जितने भी लोग मेरे देखने में आए हैं उनमें से किसी जैसा मैं नहीं हूं और मेरा तो विश्वास है कि इस समय जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबमें भी किसी जैसा मैं नहीं हूं। जैसा मैं था, वैसे अपने को दिखलाया है—नीच और घृणास्पद, भला, उच्चाशय और उदात्त—जैसा भी था वह सब। एकत्र हों मेरे चारों ओर मेरे अनगिनत साथी और सुनें मेरी आत्मस्वीकृति—मेरी अरोग्यताओं पर सिर धुनें और मेरी अपूर्णता पर शरमाएं। और फिर उनमें से हर एक स्पष्टता के साथ, सिंहासन के चरणों में अपने हृदय के रहस्यों का उद्घाटन करे और यदि साहस हो तो कहे कि मैं इस आदमी से अच्छा हूं।’’
चुनौती का ऐसा अकुंठित स्वर हिन्दी छायावाद में नहीं सुना गया; यदि ऐसी चुनौती हिन्दी में कोई दे सकता था–और एक हद तक दी भी—तो एक निराला !
ऐसे युग में जबकि विचारों और भावों को हज़ारों-लाखों आदमियों तक पहुंचाने के साधन जुट गए हों, आत्माभिव्यक्ति की स्वाधीनता स्वभावतः व्यक्ति की स्वाधीनता का बीज-मंत्र बन जाती ! सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार और छापे की मशीन की स्थापना–ये दो ऐसे साधन हैं जिन्होंने पढ़ने और लिखने की अधिक से अधिक सुविधा जुटा दी। नई शिक्षा ने अधिक-से-अधिक पाठक तैयार कर दिए और प्रेस ने उन पाठकों तक अपने विचार पहुंचाने का सुभीता जुटा दिया। बस, व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वाधीनता मांग ली। मध्ययुग में यह सुविधा न थी, इसीलिए यह स्वाधीनता भी कम थी—न तो इसकी मांग थी और न उस मांग की पूर्ति। इसी को राजनीति, दर्शन और कविता में व्यक्तिवाद की संज्ञा दी गई। छायावादी कविता का आरंभ इसी व्यक्तिवादी भावना से हुआ।
सामंती रूढ़ियोंवाले समाज के सामने जब एक पुरुष की यह स्थिति है, तो इस पुरुष-समाज में नारी के लिए आत्माभिव्यक्ति में कितनी बड़ी कठिनाई हो सकती है,यह सहज अनुमेय है। फिर भी महादेवी वर्मान ने अपने गीतों में वैयक्तिक ढंग से अभिव्यंजना की और इसके लिए उन्होंने कितने प्रवाद झेले, इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। महादेवीजी ने कहीं लिखा है कति आज का साहित्यकार अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है।
इतना होते हुए भी सामाजिक रूढ़ियों के प्रहार की आशंका से कवि को वैयक्तिक अनुभूतियों के लिए रहस्यवाद का आश्रय लेना पड़ा। स्थूल धार्मिक आवरण तो वह ले नहीं सकता था, लेकिन ऐहिक वैयक्तिकता की क्षुद्रता से बचाने के लिए रहस्यात्मकता के ऊर्ध्व आसन पर प्रिय को बैठाना ही पड़ा। महादेवी ने नारी होकर ऐसा किया तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष होकर भी प्रसाद ने ‘आंसू’ के दूसरे संस्करण को अत्यधिक रहस्यात्मक और सामाजिक लोक-मंगल-परक बना डाला; जबकि ‘आंसू’ का प्रथम संस्करण शुद्ध ऐहिक प्रेम की विरह-वेदना का काव्य है।
इतना होते हुए भी आलोचकों से वास्तविकता छिपी न रह सकी और शुक्लजी जैसे गंभीर आचार्य भी खुल ही पड़े कि ‘‘इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस-प्रसार के लिए रहस्यवाद का परदा मिल गया अथवा यों कहें कि इनकी नारी प्रणयानुभूति ससी में कूदकर असीम पर जा रही।’’
इस कथन के पीछे और प्रवृत्ति चाहे जो हो, लेकिन इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि उस युग की पुरानी पीढ़ी के लोग भी छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं को मूलतः कवि की आत्मानुभूति ही मानते थे।
यह आत्माभिव्यक्ति की भावना इस युग में कितनी व्यापक रही है, इसका पता इसी से चलता है कि ‘आत्मकथा’ लिखने की परंपरा सी चल पड़ी। गांधी, नेहरू, रवींद्रनाथ, श्रद्धानंदज, श्यामसुंदरदास, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन आदि न जाने कितने राजनीतिज्ञों, धर्मसुधारकों और साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा अथवा जीवन-स्मृति लिखी है। इतने बड़े पैमाने पर इस देश में आत्मकथाएं पहले शायद ही कभी लिखी गईं। मध्ययुग के हिन्दी साहित्य में केवल एक आत्मकथा मिलती है, बनारसीदास जैन की ‘अर्धकथानक।’
ये आत्मकथाएं इस युग में प्रचलित वैयक्तिक आत्माभिव्यक्ति की आकांक्षा की द्योतक हैं। ये बतलाती हैं कि व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कितना आकुल था ! वह अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहता था। उसकी इस आकांक्षा में स्वाधीनता की कामना थी और अभिव्यंजना में साहस भी। हर देश में ‘रौमैंटिसिज़्म’ का अभ्युदय प्रायः इसी आकांक्षा के साथ हुआ। फ्रांस और फिर पूरे यूरोप में रोमांटिक साहित्य का प्रवर्तन करनेवाले रूसो के ‘कन्फेशन’ के आरंभिक उद्गार से इस भावना के ऐतिहासिक महत्तव का ठीक पता चलता है। रूसो लिखता है :
‘‘आज मैं अपने हाथ में वह कार्य ले रहा हूं, जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया था और न भविष्य में ही कोई करेगा। मैं अपने मित्रों के सामने एक मनुष्य का सच्चा रूप रखना चाहता हूं और वह मनुष्य स्वयं मैं हूं। जितने भी लोग मेरे देखने में आए हैं उनमें से किसी जैसा मैं नहीं हूं और मेरा तो विश्वास है कि इस समय जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबमें भी किसी जैसा मैं नहीं हूं। जैसा मैं था, वैसे अपने को दिखलाया है—नीच और घृणास्पद, भला, उच्चाशय और उदात्त—जैसा भी था वह सब। एकत्र हों मेरे चारों ओर मेरे अनगिनत साथी और सुनें मेरी आत्मस्वीकृति—मेरी अरोग्यताओं पर सिर धुनें और मेरी अपूर्णता पर शरमाएं। और फिर उनमें से हर एक स्पष्टता के साथ, सिंहासन के चरणों में अपने हृदय के रहस्यों का उद्घाटन करे और यदि साहस हो तो कहे कि मैं इस आदमी से अच्छा हूं।’’
चुनौती का ऐसा अकुंठित स्वर हिन्दी छायावाद में नहीं सुना गया; यदि ऐसी चुनौती हिन्दी में कोई दे सकता था–और एक हद तक दी भी—तो एक निराला !
ऐसे युग में जबकि विचारों और भावों को हज़ारों-लाखों आदमियों तक पहुंचाने के साधन जुट गए हों, आत्माभिव्यक्ति की स्वाधीनता स्वभावतः व्यक्ति की स्वाधीनता का बीज-मंत्र बन जाती ! सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार और छापे की मशीन की स्थापना–ये दो ऐसे साधन हैं जिन्होंने पढ़ने और लिखने की अधिक से अधिक सुविधा जुटा दी। नई शिक्षा ने अधिक-से-अधिक पाठक तैयार कर दिए और प्रेस ने उन पाठकों तक अपने विचार पहुंचाने का सुभीता जुटा दिया। बस, व्यक्ति ने अपनी अभिव्यक्ति की स्वाधीनता मांग ली। मध्ययुग में यह सुविधा न थी, इसीलिए यह स्वाधीनता भी कम थी—न तो इसकी मांग थी और न उस मांग की पूर्ति। इसी को राजनीति, दर्शन और कविता में व्यक्तिवाद की संज्ञा दी गई। छायावादी कविता का आरंभ इसी व्यक्तिवादी भावना से हुआ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book